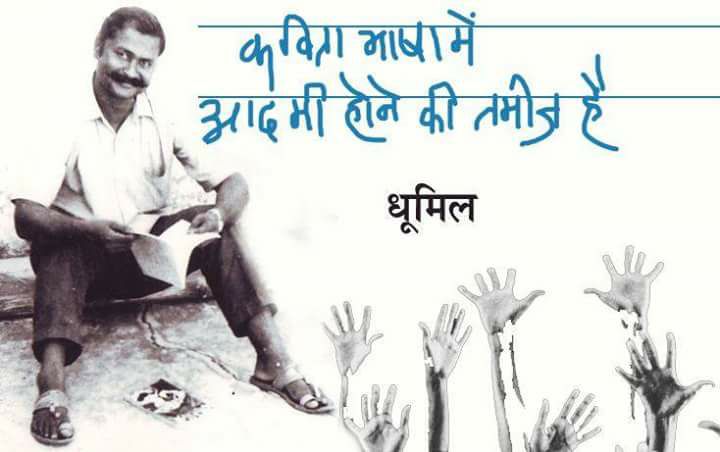मैंने
अपने यहाँ की धांधली को
बहुत गहरे जाकर महसूस किया है. मेरे जैसा आदमी, जो ईमानदारी तथा
देश निष्ठा का एकतरफा दवा
करता है, जब यहाँ होने
वाली वैधानिक धांधलियों को देखकर भी
चुप रह जाता है,
तो अचानक कई तरह के
सवाल मन में पैदा
होता है. क्या ये मेरी अपनी
कमजोरी है कि मैं
उन बेईमान लोगो का खुलकर विरोध
नहीं कर पता ? आखिर
यह क्यों है ? अपनी प्राथमिक योग्यताओं के प्रमाणपत्रों की
कमी मुझे इस वक्त बुरी
तरह खलती है. इतनी काम योग्यता वाले आदमी को जो सुविधा
यह सरकारी नौकरी दे रही है
वह शायद और नहीं मिलेगी
( जैसा की बेकरी का
दिन है ) और यही वजह
है कि मैं बहार
कर दिए जाने के डर से
चुप रह जाना अच्छा
समझता हूँ. क्योकि बात उठने पर मेरे वह
साथी, जो आड़ में
इन बुराइयों और बेईमानियों से
अपना विरोध व्यक्त करते है, शायद ही मेरा साथ
दे. वे उन्ही बेईमान
लोगो का पक्ष लेंगे,
क्योकि वे भी मेरी
तरह काम योग्यता के प्रमाण पत्र
वाले सुविधा भोगी है. परिणाम होगा कि बात उठाने
के लिए तो उठ जाएगी,
मगर वो प्रमाणित हो
पायेगी इसमें मुझे संदेह है. जहाँ तक जनतांत्रिक न्याय
पद्दति का सवाल है,
इस देश का कानून 'अपराधी'
को भी बचत की
उतनी और वैसी ही
सुविधा देती है, जैसा और जितनी एक
निर्दोष को. फिर इसके साथ यह स्पष्ट हो
चला है ( भले ही न्याय और
सत्य की घोषणायें भौकते
रहे) कि इस देश
में अपराधी वर्ग के पास इतनी
सुविधा और साधन तो
है ही कि वे
न्यायलय के कटघरे में
खड़े होने से पूर्व अपनी
क़ानूनी सुरक्षा का बंदोबस्त आसानी
से कर ले. दिक्कत
उस समय और बढ़ जाती
है कि असल अपराधी
कभी मुकाम पे नहीं आता.
वह अपने पूर्णतः सुरक्षित संवैधानिक नेपथ्य में रह कर कार्य
सञ्चालन करता है. वह साधारण और
निरपराध वर्ग के लोगों से
ही अपने कार्यक्रम अनुरूप 'व्यक्तियों' का चुनाव करता
है. कभी विशेष सुविधाओं कि लालच देकर
या कभी उसकी किसी साधारण अपराध भावना का भय दिखा
कर. और इस प्रकार
अब हम पते है
कि अपने आप में ही
हम स्थानिक क्रियाओं के साझीदार हो
गये है. जनतंत्र की - हमारे देश के जनतंत्र की
सबसे बड़ी ट्रेजडी यह है कि
हम अपने आप में अभियुक्त
और अभियोक्ता दोनों है. चुनावों ने हमारे चुनाव
करने के बोध को
ही भ्रमित कर दिया है.
जिससे असल और नक़ल,
अपराधी और अभियोक्ता के
बीच कोई निर्णायक रेखा नहीं खींची जा सकती.
मैं
अक्सर अपने लोगों के बावत सोचा
है. देर - देर तक उनसे बहसें
की है. अपने जैसे लोगो की पस्त हिम्मती
और कमजोरियों से, एकजुट होकर काम करने की योजनाओं की
लाभ से, भाषा, धर्म, देश, कानून, जाति और ना जाने
कितने दूसरे शब्दों से घंटों खींचतान
की है. मगर अंत सिर्फ वही, सुविधा पाकर जीते हुए लोगों की लाचारी. वे
एक अगुआ चाहते है. इसकी वे पूरे पैतरे
से मांग करते है. वे ईमानदारी के
नाम पर एक आदमी
की आर्थिक हत्या की योजना पर
दस्तखत करते है. मगर सामने नहीं आना चाहते. उसके लिए जवाबदेह नहीं बनना चाहते. सारी लड़ाई पर्दे
के पीछे लड़ने की राय पर
वे सहमत है. और एक दस्तखतनुमा
शब्द का त्याग करके
अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो
जाना चाहते है. उन्होंने छोटे - छोटे सिद्धांतो पर मरने वाले
लोगो के किस्से जबानी
याद कर रखे है.
बगैर यह ध्यान दिए
कि उन दिनों समय
कितना स्थिर था. मूल्य कितना मानी रखते थे. वे आज के
सन्दर्भ में भी उठी रोमानी
'बलि-वाद' को चलाने में
विश्वास रखते है और जैसे
ही उनसे मतभेद होता है, वे अपनी औकात
पे उतर आते है. ये मध्य वर्ग
के मध्यवर्गी लोग कितनी आसानी से पूरी भीड़
में एक दूसरे का
अपमान शब्दों कि मर्यादा से
नीचे आकर कर सकते है,
देख कर हैरत नहीं
होती है. दरअसल, वैतनिक सुविधाभोगी या श्रमिक मजदूर
की यह परंपरा रही
है कि वह अपनी
आवश्यकताओं के सन्दर्भ में
जितना शब्द - दारिद्र रहा है, एक दूसरे को
नंगा करने के मामले में
उतना ही वाक्यपटु. गालियों
के लिए उसे परंपरा के प्रति नत
होना नहीं पड़ा है. वे उसे अयाचित
मिली है. और उसके रक्त
में शरीक होकर उसकी सांसो का हिस्सा बन
गई है. ईश्वर उनके लिए, हमेशा एक गलत माध्यम
के रूप में सहता चला गया है.
कथाकथित
समाजवाद, अब एक सामाजिक
मजाक होकर रह गया है.
अपने
भीतर हम सभी ने
सामूहिक रूप से 'निर्ममता' पैदा करने में महारत हासिल की है,जिसके
जरिये बड़े आराम से अपने बगल
में पड़े एक भूखे और
नंगे, उपेक्षित प्राणी को नकार सके.
नकारते हुए भी उसे अपने
सामानांतर का मतदाता माने.
उसे इस देश की
जनसंख्या की एक महत्वपूर्ण
इकाई भी स्वीकारें.
भाषा,
धर्म और संस्कृति के
नारों के पीछे एक
आवेश पैदा करे और भीड़ का
दोमुहाँ रूख अपने लाभ की तरफ मोड़
दे.
भाषा,
धर्म और संस्कृति जैसे
शब्दों पर, उसके समसामायिक मुहावरों पर मैंने अक्सर
उन लोगो को पूरी उत्तेजना
से बात करते हुए देखा है और शतप्रतिशत
अकर्मण्यता की जिंदगी गुजारते
हुए शतप्रतिशत सुविधाभोगी है. और जो असल
में कामगार है, जिनको भाषा के अंधेरों में
लूटा जा रहा है,
जिनकी नीली नसों वाली मुट्ठियों में धर्म का सुदृढ़ दंड
अब भी फहरा रहा
है, जिनकी क्षुधाकुल डबडबाई हुई आँखों में पूरे देश की संस्कृति सुरक्षित
है, वे चुप है.
वे नंगे अर्धशिक्षित, भूखे कामगार, जिनकी किस्मत का पता नहीं,
किस सामाजिक नियंत्रण और भविष्य के
संयोजन की आशा में
सभी अत्याचारों और अपमान की
क्रूरताओं को तटस्थ होकर
सह रहे है.